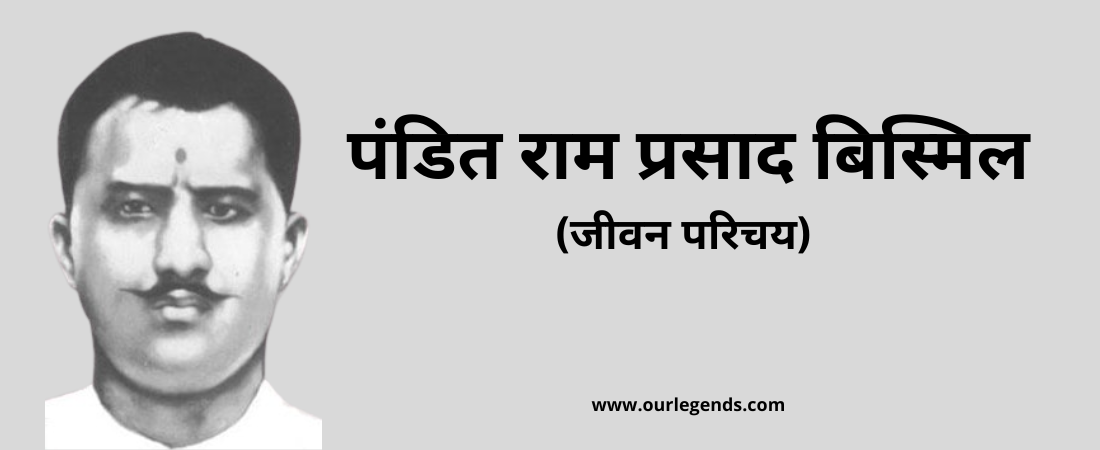पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून, 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ। वे एक प्रमुख क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने देशभक्ति की प्रसिद्ध पंक्तियों “सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजूएँ कातिल में है।” की रचना की। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम महान स्वतंत्रता सेनानियों में प्रमुखता से लिया जाता है, जिन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए शहादत प्राप्त की। वे एक उत्कृष्ट लेखक और कवि भी थे। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण सरकार ने उन पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुनाई। उन्होंने अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया।
Ram Prasad Bismil Biography, Ram Prasad Bismil ka Jivan Parichay, Ram Prasad Bismil Life, Ram Prasad Bismil Organization, Ram Prasad Bismil Inspiration
रामप्रसाद बिस्मिल का जीवन परिचय (Ram Prasad Bismil Biography In Hindi):
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून, 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ। उनकी माता का नाम मूलमती और पिता का नाम मुरलीधर था। बिस्मिल एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक माने जाते हैं।
राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन सभी भारतीयों के लिए प्रेरणादायक है। उन्हें एक साहसी स्वतंत्रता सेनानी, दूरदर्शी कवि और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की अदम्य भावना का प्रतीक माना जाता है। उनकी विरासत हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने और एक स्वतंत्र राष्ट्र के गर्वित नागरिक के रूप में एकजुट होने के लिए प्रेरित करती है।
बिस्मिल के दादा नारायण लाल बरबाई गाँव में निवास करते थे, जो उस समय के ग्वालियर राज्य के चम्बल नदी के बीहड़ों के बीच स्थित तोमरघार क्षेत्र के मुरैना जिले में था, और वर्तमान में यह मध्य प्रदेश में आता है।
रामप्रसाद ने सिगरेट छोड़ने के बाद पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी ही वह अंग्रेजी के पाँचवे स्तर पर पहुँच गए। रामप्रसाद में एक अप्रत्याशित बदलाव आया था। उनका शरीर सुडौल और मजबूत हो गया था। उन्होंने नियमित रूप से पूजा-पाठ में समय बिताना शुरू कर दिया। इसी समय, उनका संपर्क मन्दिर में आने वाले मुंशी इन्द्रजीत से हुआ। मुंशी इन्द्रजीत ने रामप्रसाद को स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक “सत्यार्थ प्रकाश” पढ़ने के लिए दी और आर्य समाज के बारे में जानकारी दी।
“सत्यार्थ प्रकाश” के गहन अध्ययन ने रामप्रसाद के जीवन पर अद्भुत प्रभाव डाला। उन्होंने 1916 में, 19 वर्ष की आयु में, क्रान्तिकारी मार्ग अपनाया और अपने क्रान्तिकारी जीवन में कई पुस्तकें लिखीं, जिन्हें उन्होंने स्वयं प्रकाशित किया। उन पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त धन से उन्होंने हथियार खरीदे, और उनके जीवनकाल में कुल 11 पुस्तकें प्रकाशित हुईं।
राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म और प्रारंभिक जीवन (Birth and Early Life of Ram Prasad Bismil):
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून, 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ। उनका परिवार हिन्दू था और वे हिन्दू धर्म की सभी परंपराओं का पालन करते थे। उनके पिता, मुरलीधर, कचहरी में सरकारी स्टांप का व्यापार करते थे, जबकि उनकी माता, मूलमति, एक कुशल गृहिणी थीं।
उनके माता-पिता को पहले एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, लेकिन वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका और किसी अज्ञात बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद से ही उनके माता-पिता और दादा-दादी ने उनकी विशेष देखभाल की।
रामप्रसाद बिस्मिल के दादा जी का मूल निवास ग्वालियर राज्य में था। ब्रिटिश शासन के समय, उनका पैतृक क्षेत्र चम्बल नदी के किनारे तोमरघार प्रांत के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र के लोग निर्भीक, साहसी और अंग्रेजों को खुली चुनौती देने वाले थे।
रामप्रसाद में भी इसी क्षेत्र का खून था, जिसका प्रमाण उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया।
इनके दादाजी ने कुछ समय बाद नौकरी छोड़कर एक दुकान खोलने का निर्णय लिया, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि होने लगी। नारायण लाल ने अपने बड़े बेटे को थोड़ी शिक्षा प्रदान की और कठिन परिश्रम करके एक मकान भी खरीद लिया। बिस्मिल के पिता, मुरलीधर के विवाह योग्य होने पर उनकी दादी ने उनके मायके में विवाह संपन्न कराया। मुरलीधर ने अपने परिवार के साथ कुछ समय ननिहाल में बिताने के बाद, अपने परिवार और पत्नी को विदा करके शाहजहाँपुर लौट आए।
जब रामप्रसाद का जन्म हुआ, तब तक उनका परिवार समाज में एक प्रतिष्ठित और समृद्ध परिवार बन चुका था। मुरलीधर ने विवाह के बाद नगर पालिका में 15/- रुपये प्रति माह की नौकरी ग्रहण की, लेकिन जब वे इस नौकरी से ऊब गए, तो उन्होंने वह नौकरी छोड़कर कचहरी में सरकारी स्टॉम्प बेचने का कार्य आरंभ किया। मुरलीधर एक सच्चे दिल वाले और ईमानदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके सरल स्वभाव के कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी।
रामप्रसाद बिस्मिल की प्रारम्भिक शिक्षा (Early Education of Ramprasad Bismil):
बचपन से ही रामप्रसाद के पिता इनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे । क्योंकि वो पढ़ाई का वास्तिवक महत्व बहुत अच्छे से समझते थे अतः वो बिस्मिल की पढ़ाई को लेकर बहुत सख्त रहते और इनके द्वारा द्वारा जरा सी लापरवाही होने पर बहुत कठोरता से व्यवहार करते और इन्हें बहुत बुरी तरह से पीटते थे। उसका मन खेलने में अधिक किन्तु पढ़ने में कम लगता था। इसके कारण उनके पिताजी तो उसकी खूब पिटायी लगाते परन्तु माँ हमेशा प्यार से यही समझाती कि “बेटा राम! शिक्षा पर ध्यान दिया करो ” इस प्यार भरी सीख का उसके मन पर कहीं न कहीं प्रभाव अवश्य पड़ता। उसके पिता ने पहले हिन्दी का अक्षर-बोध कराया किन्तु उ से उल्लू न तो उन्होंने पढ़ना सीखा और न ही लिखकर दिखाया। उन दिनों हिन्दी की वर्णमाला में उ से उल्लू ही पढ़ाया जाता था। इस बात का वह विरोध करते थे और बदले में पिता की मार भी खाते थे। हार कर रामप्रसाद को उर्दू के स्कूल में भर्ती करा दिया गया।
इसके बाद इन्हें स्कूल में भर्ती कराया गया। लगभग 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल ने चौथी कक्षा को उत्तीर्ण किया। इन्होंने कम उम्र में ही उर्दू, हिन्दी और इंग्लिश की शिक्षा प्राप्त की। अपनी कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण इन्होंने आठवीं के आगे पढ़ाई नहीं की।
संगति और वातावरण का प्रभाव(Influence of Company and Environment):
लगभग 14 वर्ष की आयु में रामप्रसाद अब उर्दू के प्रेमरस से परिपूर्ण उपन्यासों व गजलों की पुस्तकें पढ़ने का आदी हो गए थे । यदि वो उपन्यासों के लिये अपने पिता से धन मांगते तो बिल्कुल न मिलता इसलिये इन्होंने अपने पिता के संदूक से पैसे चुराने शुरु कर दिये। इसके साथ ही इन्हें नशा करने और सिगरेट पीने की भी लत लग गयी। रामप्रसाद को अपने पिता की सन्दूकची से रुपये चुराने की लत पड़ गयी। चुराये गये रुपयों से उन्होंने उपन्यास आदि खरीदकर पढ़ते , नशा करते और सिगरेट पीते । चोरी का सिलसिला चलता रहा और संयोग से एक दिन रामप्रसाद को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। खूब पिटाई हुई, उपन्यास व अन्य किताबें फाड़ डाली गयीं लेकिन रुपये चुराने की आदत नहीं छूटी। जिससे घर में इनकी हरकतों पर नजर रखी जाने लगी। रामप्रसाद की सच्चाई पर से पर्दा उठने के बाद संदूक का ताला बदल दिया गया और अपनी इन्हीं गलत हरकतों के कारण ही वो लगातार मिडिल परीक्षा में दो बार फेल भी हुये। कठोर प्रतिबंधों के कारण इनकी आदतें छूटी नहीं लेकिन बदल जरुर गयी।
आत्मसुधार और आत्मविकास के प्रयास (Striving for Self-Improvement and Self-Development):
रामप्रसाद बिस्मल को सुधारने में इनकी दादी और इनकी माँ का बहुत प्रयास रहा इनकी माँ और दादी बहुत विद्वान और बुद्धिमान थी जिससे इन्हें बुरी प्रवृतियों से छुटाकारा पाने में बहुत हद तक सहायता मिली। उसी समय इनके घर के पास के ही मन्दिर में एक विद्वान पंडित आकर रहने लगे। बिस्मिल उनके चरित्र से प्रभावित हुये और उनके साथ रहने लगे। उस पुजारी के सानिध्य में रहते हुये इन्हें स्वंय ही अपने दुर्व्यसनों से नफरत होने लगी। दूसरी तरफ स्कूल में इनकी मुलाकात सुशील चन्द्र सेन से हुई। ये उनके घनिष्ट मित्र बन गये। सेन के सम्पर्क में आकर इन्होंने सिगरेट पीना भी छोड़ दिया।
मंदिर के पुजारी के साथ रहते हुये बिस्मिल ने देव-पूजा करने की पारंपरिक रीतियों को सीख लिया। वो दिन रात भगवान की पूजा करने लगे। इन्होंने व्यायाम भी करना शुरु कर दिया जिससे इनका शरीर मजबूत होने लगा। इस प्रकार की कठिन साधना शक्ति से बिस्मिल का मनोबल बढ़ गया और किसी भी काम को करने के लिये दृढ़ संकल्प करने की प्रवृति भी विकसित हुई।
आर्य समाज और ब्रह्मचर्य (Arya Samaj and Brahmacharya):
रामप्रसाद बिस्मिल अब नियमित रूप से मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने लगे थे। एक दिन मुंशी इंद्रजीत ने उन्हें पूजा करते हुए देखा और उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने बिस्मिल से मुलाकात की और उन्हें ‘संध्या-वंदना’ करने की सलाह दी। मुंशी जी ने उन्हें आर्य समाज के कुछ उपदेश देते हुए संध्या करने की विधि बताई और साथ ही स्वामी दयानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए दिया। बिस्मिल ने अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ-साथ सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करना शुरू किया। इसमें बताए गए स्वामी जी के उपायों से बिस्मिल गहराई से प्रभावित हुए। पुस्तक में स्वामी जी द्वारा बताये गये ब्रह्मचर्य के नियमों का पूरी तरह से पालन करने लगे। इन्होंने चारपायी को छोड़कर तख्त या जमीन पर सिर्फ एक कम्बल बिछाकर सोना शुरु कर दिया। रात का भोजन करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि कुछ समय के लिये इन्होंने नमक खाना भी छोड़ दिया। रोज सुबह 4 बजे उठकर व्यायाम आदि करते। इसके बाद स्नान आदि करके 2-3 घंटो तक भगवान की पूजा करने लगे। इस तरह ये पूरी तरह से स्वस्थ्य हो गये।
राम प्रसाद का आर्यसमाज के लिए पिता से विवाद (Ram Prasad’s Dispute with his Father for Arya Samaj):
स्वामी दयानंद जी के विचारों का राम प्रसाद पर अत्यधिक गहरा असर हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वे आर्य समाज के सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन करने लगे और आर्य समाज के दृढ़ अनुयायी बन गए । इन्होंने आर्य समाज द्वारा आयोजित सम्मेलनों में भाग लेना शुरु कर दिया। इन सम्मेलनों में जो भी सन्यासी महात्मा आते रामप्रसाद उनके प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुनकर उन्हें अपनाने की पूरी कोशिश करते।
बिस्मिल का परिवार सनातन धर्म में पूर्ण आस्था रखता था और इनके पिता कट्टर सनातन धर्मी थे। किसी सनातन धर्मी ने इनके पिता को बिस्मिल के आर्य समाजी होने की सूचना दे दी।उन्होंने खुद को बड़ा अपमानित महसूस किया। क्योंकि वो रामप्रसाद के आर्य समाजी होने से पूरी तरह से अनजान थे। अतः घर आकर उन्होंने इनसे आर्य समाज छोड़ देने का लिये कहा। समाज की ऊँच-नीच के बारे में बताया। लेकिन बिस्मिल ने अपने पिता की बात मानने के स्थान पर उन्हें उल्टे समझाना शुरु कर दिया। अपने पुत्र को इस तरह बहस करते देख वो स्वंय को और अपमानित महसूस करने लगे। उन्होंने क्रोध में भर कर इनसे कहा – “या तो आर्य समाज छोड़ दो या मेरा घर छोड़ दो।” इस बात पर बिस्मिल ने अपने फैसले पर अटल रहते हुये अपने पिता के पैर छूकर उसी समय घर से निकल गए । इनका शहर में कोई परिचित नहीं था जहाँ ये कुछ समय के लिये रह सके, इसलिये ये जंगल की ओर चले गये। वहीं इन्होंने एक दिन और एक रात व्यतीत की।
जब बिस्मिल घर से इस तरह चले गए तो घर में सभी लोग परेशान हो गये। जब मुरलीधर का गुस्सा शान्त हुआ तो उन्हें भी अपनी गलती का अहसास हुआ और इन्हें खोजने में लग गये। दूसरे दिन शाम के समय जब ये आर्य समाज मंदिर पर स्वामी अखिलानंद जी का प्रवचन सुन रहे थे इनके पिता दो व्यक्तियों के साथ वहाँ गये और इन्हें घर ले आये।
बिस्मिल के इस प्रकार घर से निकल जाने की घटना के पश्चात इनके पिता ने इनका विरोध करना बंद कर दिया। वे जो भी कार्य करते, उसे चुपचाप स्वीकार कर लेते । इस तरह इन्होंने अपने सिद्धान्तों पर चलते हुये अपना सारा ध्यान समाज की सेवा के कार्यों और अपनी पढ़ाई पर लगा दिया। इन्होंने अपनी क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इनका यह क्रम आठवीं क्लास तक जारी रहा।
“मातृवेदी ” क्रांतिकारी संगठन की स्थापना (Establishment of “Matrivedi” Revolutionary Organization):
1916 में बिस्मिल ने “मातृवेदी” नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। मुख्य लक्ष्य समाज और राजनीति में सकारात्मक बदलाव लाना था। उनका दृढ़ विश्वास था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान की आवश्यकता होगी, और वह भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार थे।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन (Formation of Hindustan Republican Association) (HRA):
1920 के दशक की शुरुआत में, Ram Prasad Bismil और उनके हम वतन, जिनमें अशफाकुल्ला खान सचिन्द्र नाथ सान्याल और चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे, HRA की स्थापना के लिए एक साथ आए। संगठन का उद्देश्य सशस्त्र प्रतिरोध और क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। बिस्मिल का दृढ़ विश्वास था कि स्वतंत्रता केवल बलिदान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है और वह अपना जीवन इस उद्देश्य के लिए समर्पित करने को तैयार थे।
1922 में महात्मा गाँधी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के कारण रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने नेतृत्व में संयुक्त प्रांत के युवाओं को एकत्रित करके एक क्रांतिकारी दल की स्थापना की। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल की सहमति से, 1923 में उन्होंने पार्टी के संविधान के निर्माण के लिए इलाहाबाद की यात्रा की । पार्टी के मुख्य लक्ष्यों और उद्देश्यों को पीले रंग के कागज पर लिखा गया। इसके कारण इस पार्टी को “पीला कागज संविधान” भी कहा जाता था। पार्टी की स्थापना और उद्देश्यों के निर्माण में बिस्मिल के साथ-साथ शचीन्द्र नाथ सान्याल, जय गोपाल मुखर्जी आदि शामिल थे।
क्रान्तिकारी पार्टी के सदस्यों की पहली बैठक 3 अक्टूबर 1923 को कानपुर में आयोजित की गई। इस बैठक में बंगाल के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी शचीन्द्र सान्याल को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया । रामप्रसाद बिस्मिल को शाहजहाँपुर जिले के नेतृत्व के साथ ही साथ शस्त्र विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया। सभा में समिति ने सबकी सहमति से पार्टी के नाम को बदल कर हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोशिएशन रख दिया।
काकोरी ट्रेन डकैती / कांड (Kakori Train Robbery/ Case):
स्वतंत्रता संग्राम में Bismil के सबसे उल्लेखनीय योगदानों में से एक 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती में उनकी सक्रिय भागीदारी थी। अन्य बहादुर क्रांतिकारियों के साथ, उन्होंने लखनऊ के पास सरकारी धन ले जा रही एक ट्रेन को रोक दिया। उनका उद्देश्य इस धन का उपयोग अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए करना था। हालाँकि डकैती योजना के अनुसार नहीं हुई, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया।
हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोशिएशन के सदस्यों ने 1925 में “द रिव्युनरी” नामक 4 पृष्ठों का एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे उन्होंने अपने संगठन के उद्देश्यों को जनसामान्य तक पहुँचाने के लिए पूरे भारत में वितरित किया । इस पत्र में अंग्रेजों से क्रान्तिकारी गतिविधियों के द्वारा भारत को आजाद कराने की घोषणा के साथ ही गाँधी जी की नीतियों की आलोचना की और युवाओं को इस संगठन से जुड़ने का निमंत्रण दिया था। इस घोषणा पत्र के जारी होते ही ब्रिटिश सरकार की पुलिस बंगाल के क्रान्तिकारियों की गिरफ्तारी करने लग गयी। पुलिस ने शचीन्द्र नाथ सान्याल को इस घोषणा पत्र की बहुत सारी प्रतियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। शीर्ष नेता की गिरफ्तारी के बाद संगठन की सारी जिम्मेदारी बिस्मिल पर आ गयी। संगठन के कार्यों के लिये ये ही कर्ता-धर्ता बन गये।
एच.आर.ए. के समक्ष एक साथ दोहरी चुनौती उत्पन्न हो गई। एक तरफ अनुभवी नेताओं की गिरफ्तारी, जबकि दूसरी ओर संगठन को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। जिन क्रांतिकारी लक्ष्यों के लिए संगठन की स्थापना की गई थी, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी । इसके लिये संगठन की बैठक बुलायी गयी और उसमें डकैती कर धन इकट्ठा करने का निर्णय लिया गया। लेकिन गाँवों में डाले गये डाकों से संगठन के लिये पर्याप्त हथियार खरीदने के लिये धन एकत्र नहीं हो पाता, जिससे की अंग्रेजों के खिलाफ क्रान्तिकारी गतिविधियों को कार्यरुप में परिणित किया जा सके। अतः सभी सदस्यों ने मिलकर सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनायी।
इस बैठक में रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी, अशफ़ाक उल्ला खाँ, रोशन सिंह, रामकृष्ण खत्री, शचीन्द्र नाथ बख्शी, चन्द्रशेखर आजाद आदि ने सहभागिता की। इसमें यह निर्णय लिया गया कि सभी डकैतियों का संचालन बिस्मिल द्वारा किया जाएगा । 9 अगस्त 1925 की शाम को ट्रेन से सरकारी धन लूटने की योजना पर अशफ़ाक को छोड़कर सबने सहमति दे दी और डकैती की योजना बना ली गयी। इस डकैती की योजना में 10 सदस्यों ने भाग लिया और नेतृत्व का सारा भार इनके ऊपर था।
9 अगस्त 1925 की संध्या को दल के सदस्यों ने शाहजहाँपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन के दूसरे श्रेणी की चार टिकटें खरीदीं। इनमें शचीन्द्र बख्शी, राजेन्द्र लाहिड़ी, अशफ़ाक उल्ला खाँ और बिस्मिल शामिल थे, जबकि अन्य छह साथी, जिनमें चन्द्रशेखर आजाद और रोशन सिंह भी थे, तीसरे श्रेणी में सामान्य यात्रियों के रूप में यात्रा करने के लिए बैठ गए।
लखनऊ स्टेशन पर पहुँचने से पहले काकोरी नामक स्थान पर गाड़ी को चैन खींच कर रोका गया। बिस्मिल के निर्देशानुसार बख्शी ने गाड़ी के गार्ड को कब्जें में लिया, ये स्वंय गार्ड के दर्जे से खजाने का सन्दूक निकालने के लिये गये, 2 सदस्य गाड़ी से दूर खड़े होकर 5-5 मिनट के अन्तराल पर फायर करते, ताकि गाड़ी में बैठे पुलिस वालों और यात्रियों को लगे की गाड़ी चारों तरफ से घिरी हुई है।
सभी अन्य साथी भी सावधानीपूर्वक गाड़ी में उपस्थित यात्रियों और ब्रिटिश पुलिसकर्मियों की निगरानी करने लगे। अशफ़ाक ने हथौड़े की सहायता से तिजोरी का ताला तोड़कर सभी धन को लूट लिया। लूट के कार्य की समाप्ति की सूचना अपने साथियों को देने के लिये बिस्मिल ने अपनी बन्दूक से लगातार दो फायर किये और सभी सदस्य पास के ही जंगलों में झाड़ियों में छुपकर फरार हो गये।
लेकिन चन्द्रशेखर आजाद को पुलिस जीते जी नहीं पकड़ पायी। गिरफ्तारियों की शुरुआत में तो अशफ़ाक भी फरार होने में सफल रहे लेकिन बाद में उन्हें भी कैद कर लिया गया। बिस्मिल पुलिस को चकमा देकर कुछ समय के लिये दिल्ली में भूमिगत रहे। बाद में अपने एक मित्र के यहाँ छुपे रहे। जनवरी की कड़ाके की ठंड में रात के समय ये अपने घर आये। इनके घर आने की सूचना पुलिस को गुप्तचरों के माध्यम से उसी रात मिल गयी। अगली सुबह इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया।
मुकदमें की पैरवी के दौरान बिस्मिल को पता चला कि उनकी ही पार्टी के दो सदस्यों ने दल की योजना के बारे में पुलिस को सूचना दी थी तो इन्हें बहुत गहरा आघात लगा। एच.आर.ए. के 28 सदस्यों पर मुकदमा दर्ज था जिसमें से 2 व्यक्तियों पर बिना कोई स्पष्ट कारण दिये मुकदमा हटा दिया गया, 2 अभियुक्तों को सरकारी गवाह बनाकर उनकी सजा को माफ कर दिया और मुकदमें के सेशन के समय सेठ चम्पालाल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया गया। अन्त में केवल 20 व्यक्तियों को कोर्ट में जज के सामने पेश करके मुकदमा चलाया गया और इनमें से भी शचीन्द्र नाथ विश्वास व हरगोबिन्द को सेशन अदालत ने मुक्त कर दिया। बाकि 18 बचे व्यक्तियों को सजा सुनायी गयी।
इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ सेशन कोर्ट में भारतीय कानून की धारा 121 ए, 120 बी, और 369 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। इस मुकदमे के दौरान 18 अभियुक्तों को निम्नलिखित सजाएँ सुनाई गईं:
• रामप्रसाद बिस्मिल और राजेन्द्र लाहिड़ी – पहले दो धाराओं में आजीवन काला पानी और तीसरी धारा में फाँसी की सजा।
• रोशन सिंह – पहले दो धाराओं में 5-5 साल की कैद और तीसरी धारा में फाँसी।
• शचीन्द्र सान्याल – आजीवन काला पानी की सजा।
• मन्मथ नाथगुप्त और गोविंद चरण सिंह – दोनों को 14-14 साल की कठोर सजा।
• रामकृष्ण खत्री, मुकुंदी लाल, योगोश चटर्जी और रामकुमार सिन्हा – प्रत्येक को 10 वर्ष की कठोर कैद।
• सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य – 7 साल की कठोर कैद की सजा।
• विष्णु शरण दुबलिस, प्रणवेश चटर्जी, प्रेमकिशन खन्ना, रामदुलारे त्रिवोदी और रामनाथ पाण्डेय – सभी को 5-5 साल की कठोर सजा।
• भूपेन्द्र सान्यास और बनवारीलाल (दोनों इकबाली गवाह) – प्रत्येक को धारा के अनुसार सजा।
मैनपुरी षड़यंत्र (1918) (Mainpuri Conspiracy):
रामप्रसाद बिस्मिल अपने देश के लिये कुछ भी कर गुजरने के लिये तैयार है यह जान कर स्वामी सोम देव ने इनके विचारो को कार्यरुप में बदलने के लिये आचार्य गेंदा लाल दीक्षित से मिलने की सलाह दी।।
गेंदा लाल दीक्षित जो कि उस समय उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में डीएवी पाठशाला में अध्यापक थे। बिस्मिल ने इनके साथ मिलकर ‘शिवाजी समिति’ का गठन किया। । इस समिति के माध्यम से इन्होंने इटावा, मैनपुरी आगरा और शाहजहाँपुर के युवाओं का एक संगठन बनाया। इस संगठन के लोग शिवाजी की तरह छापेमारी करके ब्रिटिश शासन में डकैतियाँ करते थे। अपने इन कार्यों के माध्यम से ब्रिटिश अधिकारियों के मन में भारतियों का खौफ पैदा करना चाहते थे।
जब बिस्मिल अपने दल के सहयोगियों के साथ मिलकर दिल्ली और आगरा के बीच एक और लूट की योजना बना रहे थे उसी समय किसी मुखबिर कि सुचना पे पुलिस ने इस क्षेत्र की तलाशी शुरु कर दी। पुलिस द्वारा अपना पीछा किये जाने पर ये यमुना नदी में कूद गये, जिस पर इन्हें मरा हुआ समझ कर पुलिस ने इन्हें खोजना बंद कर दिया। लेकिन इस तलाशी में इनके संगठन के प्रमुख नेतृत्व-कर्ता गेंदा लाल को अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने सभी के खिलाफ सम्राट के खिलाफ साजिश करने का मामला दर्ज किया है। इस मामले को “मैनपुरी षड़यंत्र” के नाम से जाना गया है। जेल में गेंदालाल को अन्य सरकारी गवाह रामनारायण के साथ रखा गया है । गेंदालाल भी पुलिस को चकमा देकर रामनारयण के साथ जेल से फरार हो गये। पुलिस ने बहुत छानबीन की लेकिन वो इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। बाद में मजिस्ट्रेट ने मुख्य आरोपी गेंदालाल और रामप्रसाद बिस्मिल को फरार घोषित करके मुकदमें का फैसला सुना दिया।
सशक्त लेखन (Strong Writing):
बिस्मिल का भारत प्रेम और क्रांतिकारी भावना उनकी सशक्त रचनाओं में अभिव्यक्त हुई। उन्होंने अनेक देशभक्तिपूर्ण कविताएँ और गीत लिखे जो आज भी स्वतंत्रता की भावना को दर्शाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक, “सरफ़रोशी की तमन्ना (Sarfaroshi Ki Tamanna)”, अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक रैली बन गई और आज भी हमारे दिलों को गर्व से भर देती है।
व्यक्तिगत बलिदान (Personal Sacrifice):
दुख की बात है कि Bismil को स्वतंत्रता के लिए अटूट संघर्ष की बड़ी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी। क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण दिसंबर 1925 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी उत्साही रक्षा के बावजूद, ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। 19 December, 1927 को बिस्मिल को गोरखपुर सेंट्रल जेल में फाँसी दे दी गई। उनके अंतिम शब्द, “हम दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, हम स्वतंत्र हैं, और हम स्वतंत्र रहेंगे,” भारत के प्रति उनकी अदम्य भावना और समर्पण को दर्शाते हैं।
भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा (Inspiration for Future Generations):
राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान और समर्पण आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्हें एक साहसी देशभक्त के रूप में स्मरण किया जाता है जिन्होंने न्याय, समानता और भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। आज, राष्ट्र उनकी स्मृति का सम्मान करता है, उनके योगदान का जश्न मनाता है, और उनके जैसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों को मान्यता देता है।
कांग्रेस की गुप्त समिति और प्रथम पुस्तक का प्रकाशन (Secret committee of Congress and publication of the first book):
रामप्रसाद बिस्मिल लखनऊ में कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेने गए। यहाँ उनकी भेंट कांग्रेस के उन सदस्यों से हुई, जो कांग्रेस के भीतर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक गुप्त समिति का गठन कर रहे थे। बिस्मिल के अन्दर जो क्रान्तिकारी विचार उमड़ रहे थे अब उन्हें क्रियान्वित करने का समय आ गया था। ये बाहर से ही इस समिति के सदस्यों के कार्यों में मदद करने लगे। इनकी लगन को देखकर गुप्त समिति के सदस्यों ने इनसे सम्पर्क किया और इन्हें कार्यकारिणी समिति का सदस्य बना लिया।
गुप्त समिति के पास सीमित वित्तीय संसाधन थे और क्रान्तिकारी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। समिति की धन की आवश्यकता को पूरी करने के लिये रामप्रसाद बिस्मिल ने पुस्तक प्रकाशित करके उसके धन को समिति के कोष में जमा करके लक्ष्यों की प्राप्ति करने का विचार प्रस्तुत किया। इससे दोहरे उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती थी। एक तरफ किताब को बेचकर धन प्राप्त किया जा सकता था, दूसरी तरफ लोगों में क्रान्तिकारी विचारों को जगाया जा सकता था।
गुप्त समिति के पास सीमित वित्तीय संसाधन थे और क्रान्तिकारी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। पुस्तक की बिक्री हो जाने के बाद इन्होंने अपनी माँ से लिये रुपये वापस कर दिये और सारे हिसाब करने के बाद में 200 रुपये बच गये जिससे इन्होंने हथियार खरीदे। पूरी किताबें अभी बिक नहीं पायी थी कि इन्होंने 1918 में ‘देशवासियों के नाम संदेश’ नाम से पर्चें छपवाये। संयुक्त प्रान्त की सरकार ने इनकी किताब और पर्चें दोनों पर बैन लगा दिया।
सरकार द्वारा प्रतिबंधित किताबों की बिक्री (Sale of Books Banned by the Government):
28 जनवरी 1918 को रामप्रसाद बिस्मिल ने जनता में क्रान्तिकारी विचारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से “देशवासियों के नाम संदेश” शीर्षक से पर्चे प्रकाशित कर अपनी कविता “मैनपुरी की प्रतिज्ञा” के साथ वितरित किए। इनकी किताब पर सरकार ने बेचने के लिये रोक लगा दी जिस पर इन्होंने अपने साथियों की मदद से कांग्रेस अधिवेशन के दौरान बची हुई प्रतियों को बेचने की योजना बनायी।
1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के समय शाहजहाँपुर सेवा समिति द्वारा एक स्वंयसेवक दल एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा गया। इस दल में बिस्मिल और उनके कुछ सहयोगी शामिल थे । स्वंयसेवकों का दल होने के कारण पुलिस ने इनकी कोई तलाशी नहीं ली और वहाँ पहुँचकर इन्होंने खुले रुप से पुस्तकों को बेचना शुरु कर दिया। पुलिस ने शक होने पर आर्य समाज द्वारा बेची जा रही किताबों की जाँच करना शुरु कर दिया। इतने में बिस्मिल बची हुई प्रतियों को एकत्र करके दल के साथ वहाँ से फरार हो गये।
रामप्रसाद बिस्मिल की भूमिगत गतिविधियाँ (Underground Activities of Ramprasad Bismil):
मैनपुरी षड़यन्त्र के प्रमुख आरोपी के रूप में भागते समय इन्होंने यमुना में कूदने का निर्णय लिया, जिसके परिणामस्वरूप इनका कुर्ता नदी में बह गया। और ये तैरकर सुरक्षित नदी के दूसरे किनारे पर चले गये। इनके कुर्तें को नदी में देखकर पुलिस को लगा कि शायद गोली लगने से इनकी मौत हो गयी है। अतः इन्हें मृत मान लिया गया। वहीं जब रामप्रसाद को ये ज्ञात हुआ कि इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है तो इन्होंने मैनपुरी षड़यन्त्र पर फैसले होने तक स्वंय को प्रत्यक्ष न करने का निर्णय किया। ये 1919 से 1920 के बीच में भूमिगत होकर कार्य करने लगे। इस बीच इन्होंने अपने किसी भी करीबी से कोई भी सम्पर्क नहीं किया।
1919-20 में भूमिगत रहते हुये राम प्रसाद बिस्मिल उत्तर प्रदेश के कई गाँवों में रहे। कुछ समय के लिये रामपुर जहाँगीर गाँव में रहे, जो वर्तमान समय में ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध जिले में आता है, कुछ दिनों के लिये मैनपुरी जिले के कोसमा गाँव में और आगरा जिले के बाह और पिन्नहट गाँवों में रहे। ये अपनी माँ से कुछ धन उधार लेने के लिये अपने पैतृक गाँव भी गये।
बिस्मिल ने भूमिगत रहते हुये अनेक पुस्तकें लिखी। जिनमें से उनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं –
- मन की लहर (कविताओं का संग्रह)।
- बोल्वेशिक की करतूत (एक क्रान्तिकारी उपन्यास)।
- योगिक साधन (आत्मचिंतन के लिये योगा को परिभाषित किया गया है)।
- स्वाधीनता की देवी या कैथरीन (रुसी क्रान्ति की ग्रांड मदर कैथरीन लिये समर्पित आत्मकथा)।
आम नागरिक का जीवन (Life of a Common Man):
1920 में सरकार ने अपनी उदारता की नीति के तहत मैनपुरी षड़यन्त्र मुकदमे के आरोपियों को रिहा करने की घोषणा की। इस घोषणा के पश्चात रामप्रसाद बिस्मिल अपने गाँव शाहजहाँपुर लौट आए और अपने जिले के अधिकारियों से भेंट की । उन अधिकारियों ने इनसे एक शपथ पत्र लिया जिस पर ये लिखवाया गया कि वो आगे से किसी भी क्रान्तिकारी गतिविधि में भाग नहीं लेंगें। इनके इस प्रकार का शपथ पत्र देने पर इन्हें अपने गाँव में शान्तिपूर्वक रहने की अनुमति मिल गयी।
बिस्मिल ने शाहजहाँपुर पहुँचने के बाद साधारण जीवन जीना प्रारंभ किया। कुछ समय के लिए वे भारत सिल्क निर्माण कम्पनी में प्रबंधक के पद पर कार्यरत रहे। इसके पश्चात, उन्होंने बनारसी दास के साथ मिलकर साझेदारी में अपना स्वयं का सिल्क निर्माण उद्योग स्थापित किया । रामप्रसाद ने कम समय में ही स्वंय को इस व्यवसाय में स्थापित करके काफी धन अर्जित कर लिया। इतना सब कुछ करने पर भी इन्हें आत्मिक शान्ति नहीं मिल रही थी, क्योंकि अभी तक ये ब्रिटिश सरकार को भारत से बाहर करने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरी नहीं कर पाये थे।
असहयोग आन्दोलन के दौरान बिस्मिल (Bismil during the Non-Cooperation Movement):
जिस समय रामप्रसाद बिस्मिल आम नागरिक के रुप में जीवन जी रहे थे, उस समय देश में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आन्दोलन चल रहा था। गाँधी जी से प्रेरित होकर ये शाहजहाँपुर के स्वंय सेवक दल के साथ अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में गये। इनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य प्रेमकृष्ण खन्ना और अशफ़ाक उल्ला खाँ भी थे। इन्होंने एक अन्य कांग्रेस सदस्य मौलाना हसरत मौहानी के साथ पूर्ण स्वराज्य की भूमिका वाले प्रस्ताव को पास कराने में सक्रिय भूमिका भी निभाई।
कांग्रेस के अधिवेशन से लौटने के पश्चात, इन्होंने संयुक्त प्रान्त के युवाओं को असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। वे विभिन्न सभाओं का आयोजन कर उनमें अपने विचार प्रस्तुत करते थे । इनके उग्र भाषणों और कविताओं से लोग बहुत प्रभावित हुये और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहसहयोग आंदोलन में भाग लेने लगे। इन कार्यों के कारण ये ब्रिटिश सरकार के शत्रु बन गये। इनकी अधिकांश पुस्तकों और लेखों को सरकार ने प्रकाशित करने व बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया।
शहादत का दिन (Ram Prasad Bismil Death):
कोर्ट की 18 महीने तक चली विस्तृत प्रक्रिया के उपरांत रामप्रसाद बिस्मिल, अशफ़ाक उल्ला खाँ, राजेन्द्र लाहिड़ी और रोशन सिंह की फाँसी की सजा को बनाए रखा गया। 19 दिसम्बर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में सुबह 8 बजे फाँसी दे दी। बिस्मिल के साथ ही अशफ़ाक को फैजाबाद जेल में और रोशन सिंह को इलाहबाद के नैनी जेल में फाँसी दी गयी। जबकि राजेन्द्र लाहिड़ी को फाँसी की निश्चित तिथि से 2 दिन पहले 17 दिसम्बर को, गोंडा जेल में फाँसी दे दी गयी।
शहीद बिस्मिल की अंतिम यात्रा (Last Journey of Shaheed Bismil):
रामप्रसाद बिस्मिल की फाँसी की खबर सुनते ही लोग उनकी जेल के बाहर लाखों की तादाद में जमा हो गए। इतनी विशाल भीड़ को देखकर ब्रिटिश जेल के अधिकारी भयभीत हो गए। उन्होंने जेल का मुख्य द्वार बन्द कर दिया। इस पर भीड़ ने जेल की दीवार तोड़ दी और रामप्रसाद बिस्मिल के पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ उनके माता-पिता के सामने लाये।
शहरवासियों को बिस्मिल के अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को गोरखपुर के घन्टाघर में रखा गया था। इसके पश्चात, इस महान क्रांतिकारी के शरीर को पूरे सम्मान के साथ राप्ति नदी के किनारे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। शहरवासियों को बिस्मिल के अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को गोरखपुर के घन्टाघर में रखा गया था। इसके पश्चात, इस महान क्रांतिकारी के शरीर को पूरे सम्मान के साथ राप्ति नदी के किनारे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इनके शोक सम्मेलन के जूलुस में हिन्दी साहित्य के महान लेखक होने के साथ ही कल्याण हनुमान प्रसाद पोद्दार के संस्थापक महावीर प्रसाद द्विवेदी और राजनीतिज्ञ गोविन्द बल्लभ पन्त भी शामिल हुये थे। वो दोनों अंतिम संस्कार की अन्तिम विधि होने तक वहाँ उपस्थित रहे थे।
‘क्रान्ति की देवी’ के साधक स्वयं देश के लिए शहीद हो गए, किंतु अपनी शहादत के साथ-साथ उन्होंने युवा क्रान्तिकारियों की एक नई पीढ़ी के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया।
रामप्रसाद बिस्मिल के साहित्यिक कार्य (Literary works of Ramprasad Bismil):
बिस्मिल न केवल एक महान क्रान्तिकारी थे, बल्कि एक उत्कृष्ट देशभक्ति कवि भी थे। उन्होंने न केवल काव्य में, बल्कि गद्य साहित्य में भी कई महत्वपूर्ण रचनाएँ कीं। अपने 11 वर्षों के क्रान्तिकारी जीवन में, उन्होंने 11 पुस्तकें लिखीं। इनमें से कुछ प्रमुख और उल्लेखनीय कार्य निम्नलिखित हैं:
सरफ़रोशी की तमन्ना (भाग-1) – बिस्मिल के व्यक्तित्व और उनके साहित्यिक योगदान का गहन अध्ययन।
सरफ़रोशी की तमन्ना (भाग-2) – संदर्भ और व्याकरण संबंधी प्रशंसा के साथ बिस्मिल द्वारा रचित लगभग 200 कविताएँ।
सरफ़रोशी की तमन्ना (भाग-3) – इस खंड में बिस्मिल द्वारा लिखी गई 4 पुस्तकों का संकलन है। ये 4 पुस्तकें हैं: निज जीवन कथा (मूल आत्मकथा), अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास, कैथरीन – स्वाधीनता की देवी (अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवादित) और यौगिक साधन (बंग्ला से हिन्दी में अनुवादित)।
सरफ़रोशी की तमन्ना।मन की लहर – ब्रिटिश शासन काल में लिखी गयी कविताओं का संग्रह।
बोल्वेशिक की करतूत – क्रान्तिकारी उपन्यास।
- क्रान्ति गीतांजलि – कविता संग्रह।
रामप्रसाद बिस्मिल के जीवन का संक्षिप्त सार (Brief Summary of the Life of Ramprasad Bismil):
पूरा नाम – राम प्रसाद बिस्मिल
जन्म – 11 जून 1897
पिता का नाम – मुरलीधर
माता का नाम – मूलमति
जन्म स्थान – शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रान्त (ब्रिटिश राज्य में)
संगठन – हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एशोसिएशन
उपलब्धी – महान क्रान्तिकारी, शहीद, लेखक व कवि
मृत्यु – 19 दिसम्बर 1927
मृत्यु स्थान – गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)
यह जीवनी सार्वजनिक स्रोतों में उपलब्ध जानकारी पर आधारित है और इसे पूरी तरह से सटीक नहीं माना गया है। उल्लेखित विवरण केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए हैं, और पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे तथ्यों की पुष्टि अपने स्वयं के शोध और विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से करें।